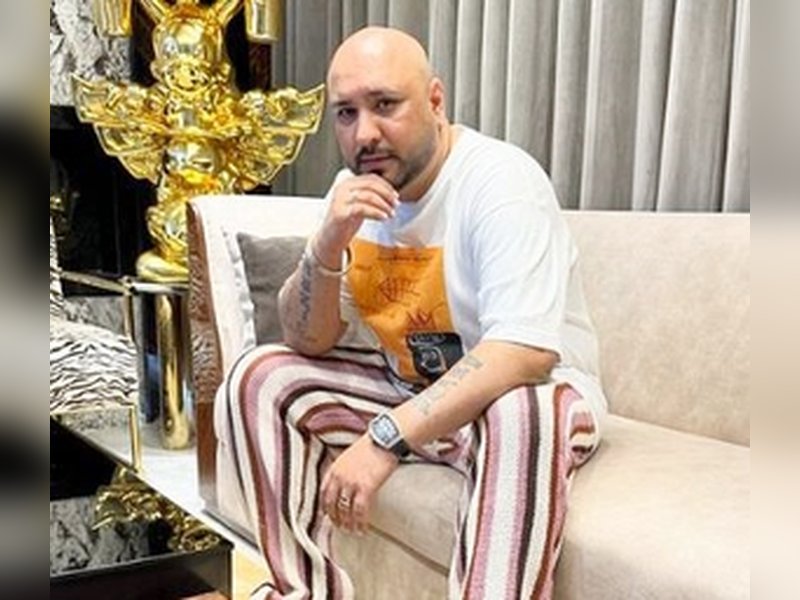नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भाषा केवल संवाद का नहीं बल्कि आपकी संवेदना और सांस्कृतिक समृद्धि का भी परिचायक है। भाषा के तौर पर आपको हमेशा यह एहसास उसमें रचे-बसे शब्दों के जरिए होता रहता है कि वह आपकी सोच और समझ को कितना प्रभावित करती है और आपके दिल को कितना छूती है। अंग्रेजी में शब्दों को एक बार गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वह शब्द आपके मन में एक सपाट स्पर्श छोड़ते हैं। ऐसा हिंदी या उर्दू जैसी भाषा के शब्दों के साथ नहीं है। इसमें हर शब्द की एक अलग संवेदना और संरचना है जो गहराई तक जाकर आपके मनोभाव पर असर करती है।
हिंदी जैसी समृद्ध भाषा के साथ उर्दू के शब्दों का घुलना एक ऐसी चासनी तैयार कर रही है जिसकी मिठास भाषा के तौर पर हिंदी को ज्यादा समृद्ध और सशक्त बना रही है। अब तो हिंदी पट्टी के क्षेत्र में जितनी क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का गठबंधन हिंदी के साथ हुआ है, उर्दू के शब्द भी उतनी ही आसानी और सहजता के साथ उसमें पिरोए हुए हैं। 9 नवंबर को जब पूरी दुनिया ने विश्व उर्दू दिवस मनाया तो यह देखना जरूरी है कि हिंदी को समृद्ध और सशक्त मनोभाव की भाषा बनाने में इसका कितना योगदान है।
दरअसल किसी भी भाषा की समृद्धि, सहजता और सरलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भौगोलिक रूप से वो कितने क्षेत्रों तक रची-बसी और बोली जाती है और कितने दिलों को छू पाती है। हिंदी और उर्दू इस मामले में बेहतरीन भाषाएं हैं। अपनी सरलता और सहजता के कारण ये भाषाएं सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी बोली जाती हैं।
हिंदी और उर्दू दोनों एक-दूसरे से काफी मिलती हैं। हिंदी साहित्य में भी उर्दू के शब्दों का बड़ी ही सहजता के साथ प्रयोग किया जाता है। 9 नवंबर के दिन जब दुनिया ने विश्व उर्दू दिवस मनाया, तो यह जानना जरूरी है कि उर्दू को एक भाषा के तौर पर दुनिया में इतनी पहचान मिली कैसे। दरअसल, अल्लामा इकबाल को तो सब जानते हैं। एक ऐसे साहित्य के सूरमा जिनकी कलम की ताकत ने पूरी दुनिया के मंच पर इस भाषा को यह पहचान दिला दी।
आईएएनएस ने इस अवसर पर एक खास पहल की। दरअसल हमने उर्दू की समृद्धि को केवल उसके साहित्यकारों के चश्मे से देखने और जानने से परहेज किया क्योंकि यह एक तरह से भाषा के लिए केवल खानापूर्ति होती और कुछ नहीं। ऐसे में हमने उर्दू दिवस के मौके पर हिंदी के लेखक और प्रकाशकों की राय ली, ताकि दिखाया जा सके कि हिंदी में उर्दू कैसे रची-बसी है और हमारी भाषा को कैसे इसने समृद्ध बनाया है। वैसे भी कहते हैं कि हिंदी उर्दू की मौसी है और मौसी को एक बार शब्द विच्छेद करके पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा मां सी यानी मौसी। मतलब एक भाषा जो पहले से समृद्ध रही उसने दूसरी भाषा के साथ मिलते समय अलगाव नहीं छोड़ा। वह उन नदियों के संगम की तरह अलग नहीं रही, जहां पानी के रंग से आप नदियों की धाराओं को पहचान लें।
उर्दू को लेकर आईएएनएस से नई वाली हिंदी साहित्य के जगमगाते सितारे 'डार्क हॉर्स' और 'औघड़' जैसी साहित्यिक कृति को अपनी कलम से पन्नों पर उकेरने वाले लेखक और कवि नीलोत्पल मृणाल ने कहा कि उर्दू ने हिंदी साहित्य को एक नमी दी है, ठीक वैसे कि जैसे सूखी जमीन पर बारिश की पहली फुहार। कबीर की सादगी और तुलसी की माटी में जब मीर, गालिब और फैज की नजाकत घुली, तो हिंदी का मुहावरा भी नरम पड़ा, और उसका लहजा भी मोहब्बत-भरा हुआ आया।
वह कहते हैं कि आधुनिक लेखन में भी उर्दू एक प्रभावी भाव का माध्यम बन चुकी है। इसमें न अतीत की दीवार है, न वर्तमान की दूरी। हिंदी कविता में उर्दू शब्द वैसे ही हैं, जैसे चाय में इलायची की सुगंध। हर बार जरूरी नहीं, लेकिन जब आते हैं, पूरी अनुभूति बदल देते हैं। ‘मोहब्बत’ शब्द में जो लय है, उसे केवल हिंदी शब्द ‘प्रेम’ से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तन्हाई में जो रूहानीपन है, वह अकेलेपन में नहीं, बल्कि उर्दू के शब्दों में महसूस होता है। यही कारण है कि हिंदी कविता में उर्दू शब्दों से नजाकत, तहज़ीब और रूह की खुशबू आती है।
हिंदी जैसी समृद्ध और बहुप्रभावी भाषा के पास भावनाओं और अभिव्यक्ति के सारे औजार हैं, लेकिन उर्दू ने इसे और समृद्ध किया है। उर्दू के शब्द और भाव हिंदी कविता को प्रेम, दर्द, इंसानियत और सामाजिक चेतना दोनों की गहराई देते हैं। यह हिंदी और उर्दू के बीच का पुल है, जो दिल और दिमाग की आवाजाही दोनों को सहज बनाता है।
वह कहते हैं कि हिंदी और उर्दू की लिपि अलग है। हिंदी देवनागरी में सांस लेती है और उर्दू फारसी-नास्तालिक में धड़कती है, लेकिन भाषा की आत्मा एक ही है। जैसे दो भाई अलग घर में रहते हुए भी मां की रसोई की खुशबू साझा करते हैं, वैसे ही हिंदी और उर्दू का दिल एक है। रोजमर्रा की बातचीत में हम जो बोलते हैं, वह हिंदुस्तानी है, ना शुद्ध हिंदी, ना शुद्ध उर्दू।
नीलोत्पल मृणाल कहते हैं कि नई हिंदी सिर्फ दिल्ली या बनारस की नहीं है। यह हिंदी है जो बिहार, झारखंड, राजस्थान, मुंबई और लखनऊ की बोली का मिश्रण है। इसमें मैथिली की मिठास, भोजपुरी की ठसक, मराठी का कर्रापन और उर्दू की नजाकत एक ही वाक्य में मिल जाती है। यही विविधता हिंदी की ताकत है। हिंदी अगर गंगा है, तो उर्दू उसकी यमुना है।
उनका मानना है कि भाषाओं को अलग करना केवल राजनीतिक दृष्टिकोण है, सांस्कृतिक नहीं। हिंदी और उर्दू का बचपन एक ही आंगन में बीता, उनकी आत्मा एक जैसी है। लिपि की दीवार केवल यह भुलाने की कोशिश है कि ये दोनों भाषाएं एक-दूसरे की सहेली हैं। हिंदी और उर्दू की आपसी दोस्ती को समझने के लिए यह जरूरी नहीं कि हर शब्द का स्रोत पहचाना जाए। इसका अनुभव रोजमर्रा की बोली और साहित्य में महसूस किया जा सकता है।
साहित्यकार विजयश्री तनवीर इसे गंगा-जमुनी तहज़ीब का पर्याय मानती हैं। वह कहती हैं कि कबीर और जायसी ने हिंदी और उर्दू की साझी विरासत हमें सौंप दी। खड़ी बोली में लिखा गया साहित्य उर्दू की नींव पर खड़ा है। उर्दू ने हिंदी को हजारों शब्द दिए। ‘हिन्दवी’ और ‘हिंदुस्तानी’ जैसे शब्द दोनों भाषाओं को फलने-फूलने का अवसर देते हैं। एक बार दूध और पानी मिल जाए, तो वे अलग नहीं होते, उर्दू और हिंदी का भी यही हाल है।
वह कहती हैं कि हिंदी साहित्य उर्दू से अछूता नहीं है। हिंदुस्तानी बोली में उर्दू की भरमार स्वाभाविक है। मीर, इकबाल और गालिब की परंपरा आज भी कई लेखकों में जीवित है। फिराक गोरखपुरी, आनंद नारायण मुल्ला, कृष्ण चंदर, कुंवर बेचैन, कुंवर नारायण और गुलज़ार सभी ने हिंदी-उर्दू की गंगा-जमुनी भाषा में लेखन किया। हिंदी गीतों में उर्दू ने इतनी रूमानियत, मिठास और भाव भरी है कि उनके बिना गीत अधूरे लगते हैं।
हिंदी की लिपि देवनागरी है और उर्दू की नास्तालिक। लेकिन व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण में समानता है। दोनों की जड़ खड़ी बोली है और दिल्ली-लखनऊ जैसी जगहों में उनका अंतर पहचानना मुश्किल है। प्रेमचंद का साहित्य इसका सजीव उदाहरण है। उनके पहले कहानी संग्रह ‘सोज ए वतन’ और उपन्यास ‘असरारे मआबिद’ उर्दू में थे। हिंदी साहित्य में उर्दू की डूब इतनी गहरी है कि उसके बिना हिंदी की रचना अधूरी है।
वहीं, 'ओ रे! किसान' और 'मैं से मां तक' की लेखिका अंकिता जैन इसे दो जुड़वां बहनों के रूप में देखती हैं, इतनी गहरी आपसी मित्रता कि उन्हें अलग करना असंभव है। उनके मुताबिक, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनजाने ही उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ‘रास्ता’, जो मूलतः फारसी शब्द है, पर अब हिंदी का अभिन्न अंग बन चुका है। यह साबित करता है कि हिंदी और उर्दू के बीच कोई भूमिका तय करने की आवश्यकता ही नहीं है। वे अब हिंदी साहित्य और भाषा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं।
नई हिंदी आज की हमारी हिंदी है। यह क्षेत्रीय भाषाओं, उर्दू और अंग्रेजी के प्रभावों का मिश्रण है। लेखकों को चाहिए कि वे उर्दू का प्रयोग शऊर और सजीवता से करें, न कि जबरदस्ती। यही भाषा को जीवंत और मोहक बनाए रखता है।
लब्बो-लुबाब यह है कि हिंदी और उर्दू के बीच बहस और विवाद बेकार है। पाठ्यक्रम बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर हमारी यह सांस्कृतिक धरोहर हमें बचाए रखनी है। हिंदी और उर्दू का संगम हमारे दिल और सोच की एकता का प्रतीक है। इनके शब्द, भाव और लय हमारे साहित्य, गीत और बोली में हमेशा जीवित रहेंगे।
अंकिता जैन कहती हैं कि हिंदी और उर्दू सिर्फ भाषाएं नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत हैं। वे हमारे भीतर उसी तरह बहती हैं जैसे गंगा और यमुना का संगम। उनका मेल हमारी संस्कृति, हमारी कविता और हमारी बोली की आत्मा है। आज भी, हर हिंदी-उर्दू शब्द में वह मिठास, वह मोहब्बत, वह इंसानियत और वह गहराई महसूस होती है, जो हमारी भाषा को विश्वभर में अनोखा और अमूल्य बनाती है।
--आईएएनएस
पीआईएम/एबीएम