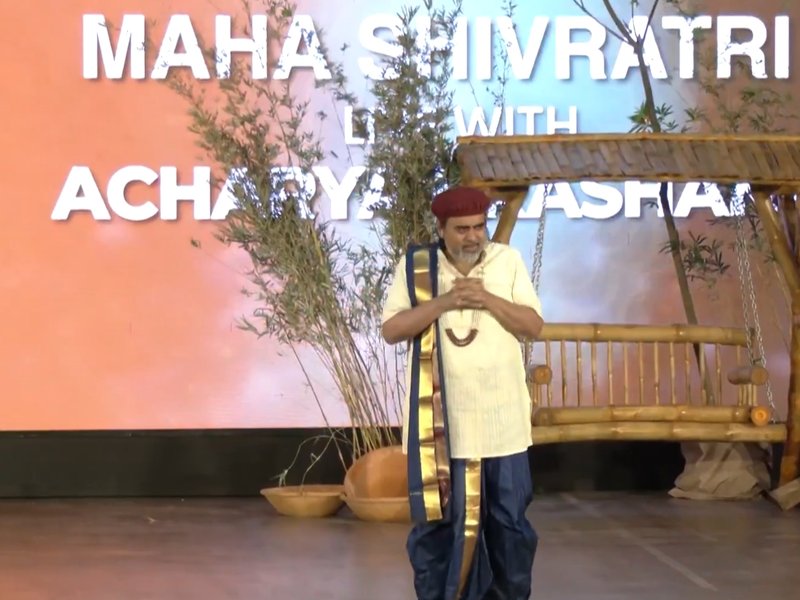नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। लोकपर्व छठ अब ग्लोबल हो गया है। बिहार या पूर्वांचल के लोग दुनिया के जिस भी कोने में बसे हैं बड़े शान और सम्मान से छठी मईया को पूजते हैं। पर्व की आहट के साथ ही गांवों की पगडंडियां, तालाबों के किनारे, मिट्टी के आंगन और नदी के घाट किसी अनदेखे सुर से भर उठते हैं।
यह कोई शोर नहीं होता, न ही माइक पर चढ़ा लाउडस्पीकर। यह होती है मांओं और बहनों की धीमी, गहरी, आत्मा तक उतर जाने वाली लोकधुन— “केरवा से फलेला घेवद से…”। इन गीतों में न देवता का कोई औपचारिक नाम होता है, न वेद-मंत्रों का वैभव, लेकिन फिर भी इनमें एक पूरा ब्रह्मांड बसता है: जल, जंगल, जड़, जन और जननी। छठ के ये लोकगीत उस भाव का परिचय हैं जहां पूजा शब्दों से नहीं, सुरों से होती है।
छठ का व्रत सिर्फ नियमों और कठोर संकल्प का ही नहीं बल्कि संवाद का पर्व है— प्रकृति से संवाद, पूर्वजों से संवाद, और अंततः उस अदृश्य शक्ति से संवाद जिसे लोग सूर्य कहते हैं पर महसूस मातृभाव की तरह करते हैं। जब व्रती महिला “हे छठी मइया, तोहार महिमा अपार…” गाती है, तो वह सिर्फ एक देवी को नहीं पुकारती, वह अपनी हर चिंता, हर आशंका और हर उम्मीद उसी धुन में बांध देती है। ये गीत किसी रेडियो या किताब से नहीं आते, ये पीढ़ियों की गोद में पले होते हैं।
लोकगीतों में छठ की सबसे बड़ी खूबी प्रकृति का मानवीकरण है। नदी को बहन कहा जाता है, सूरज को भाई, और सांझ को कोई थका हुआ यात्री। जैसे एक गीत में कहा जाता है, “गंगा मइया तोहार आरती उतारब…” — यहां गंगा कोई जलधारा नहीं, बल्कि एक मां है जिसकी गोद में समर्पण होता है। यह वही भाव है जो लोकमन को धर्म से नहीं, धरती से जोड़ता है। छठ का गीत बताता है कि पूजा खेत की मेड़ पर भी की जा सकती है।
इन गीतों में स्त्रियों का दर्द भी होता है और अद्भुत धैर्य भी। कई बार गीत में व्रती अपने रिश्ते की गरिमा का ध्यान रखते हुए ताने भी देती है। कहती है, “तू त आन्हर हुईहे रे बटोहिया, इ दल तोरा न बुझाए।” यह कोई मंत्र नहीं, लेकिन इससे बड़ी प्रार्थना कौन-सी हो सकती है?
जब लकड़ी के चूल्हे पर ठेकुआ पकता है और आंगन में धुआं घुलता है, तभी ऐसी कोई धुन उठती है जिसमें पूरे घर की चिंता घुल जाती है। छठ के गीत बताते हैं कि स्त्री सिर्फ व्रती नहीं, वह इस पर्व की कवयित्री भी है।
सबसे अनोखी बात यह है कि ये लोकगीत कभी एक जैसे नहीं रहते। हर गांव में, हर घर में, हर मां अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसमें कुछ जोड़ती-घटाती रहती है। कभी बेटी के विवाह की चिंता, कभी बेटे की नौकरी की आस, कभी घर की गरीबी का दुख, सब कुछ सुर बनकर बहता जाता है।
शहरों में जब छठ मनाया जाता है, तो यह लोकगीत ईयरफोन या रिकॉर्डिंग से नहीं गाए जाते। भले ही सब कुछ प्लास्टिक के टेंट में हो, घास के मैट की जगह तरपाल हो, लेकिन एक व्रती मां की आवाज जैसे ही उठती है- “उठ ए सूरज मल, कर अरघ स्वीकार…”, तो अचानक पूरा दृश्य गांव बन जाता है। कोई पुल के नीचे अस्थायी घाट बनाता है, कोई बाल्टी में जल भरकर ही आसमान की ओर देखता है, लेकिन गीत वही होता है जिसके तार सदियों से जुड़े हैं।
इन लोकगीतों में एक गूढ़ तत्व और है- आसक्ति और विरक्ति का संगम। त्योहारों में जहां बाजार अब पूजा का सामान तय करता है, वहां छठ के गीत आज भी बताते हैं कि कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं जा सकते।
शायद इसी इसलिए कहा जाता है— छठ पूजा में मूर्ति नहीं होती, पर भक्ति की सबसे सजीव प्रतिमा यहीं दिखती है। न फूलों का जंगल, न घंटों की गूंज— केवल मिट्टी, जल और मानवीय स्वर का संगम। छठ के लोकगीत हमें यह याद दिलाते हैं कि भक्ति जब भाषा छोड़कर भाव बन जाए, तो वह नदी की तरह बहती है, हवा की तरह गाती है।
आज भी जब तालाबों के किनारे अंधेरा उतरता है और व्रती स्त्री जल में खड़ी होकर धुन उठाती है, तो लगता है जैसे सैकड़ों वर्षों की विरासत एक ही सांस में समा गई हो। सूरज की पहली किरण का इंतजार करते हुए गाती है- "कब उगिहें चकवा कब मारब फकवा" एहसास दिला देती है कि वो अरघ की प्रतीक्षा तो कर रही है लेकिन साथ ही अपनी तपस्या का एहसास भी करा देती है।
सूर्योदय के क्षण में कोई भक्त नहीं, केवल एक मां दिखती है, जो उनके उगते ही सोहर गाकर छठी मईया को बधाई देती हुई आगे बढ़ जाती है।
--आईएएनएस
केआर/